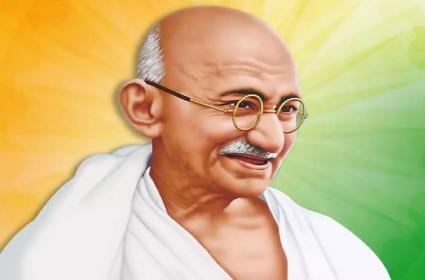
पवन वर्मा
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज के प्रत्येक आयाम पर गहन विचार किया। चाहे स्वराज की परिकल्पना हो, ग्राम स्वावलंबन का विचार हो या शिक्षा की दिशा, गांधीजी हर क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तनकारी दृष्टि लेकर आए। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है। उन्होंने जिस ‘बुनियादी शिक्षा’ की संकल्पना रखी, वह केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित न होकर जीवन के हर पहलू को छूने वाली थी। गांधीजी ने कहा था कि- “शिक्षा का उद्देश्य केवल दिमागी विकास नहीं है, बल्कि मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। आज जब हम बेरोजगारी, कौशलहीन डिग्रियों, शिक्षा में बाजारवाद और बच्चों पर सूचना का अनावश्यक बोझ देखते हैं, तब गांधीजी की बुनियादी शिक्षा की प्रासंगिकता और अधिक गहराई से सामने आती है। गांधीजी ने शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान या परीक्षा पास करने का साधन नहीं माना। उन्होंने 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में अपनी अवधारणा स्पष्ट की। उनका मानना था कि हमारी शिक्षा स्वावलंबी हो ,यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति जीवनयापन के योग्य बने। शिक्षा क्रियात्मक और उत्पादक हो जिससे बालक अपने हाथों से कार्य करके सीखे। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए ताकि बालक सहज रूप से ज्ञान अर्जित कर सके। शिक्षा में चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों पर अनिवार्य रुप से ध्यान हो। गांधीजी का मानना था कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा बच्चों की प्रवृत्ति, सृजनशीलता और स्वाभाविक विकास के अनुरूप होनी चाहिए। बच्चे करके सीखें, अनुभव से समझें और श्रम को सम्मान दें। बालकों के स्वाभाविक विकास और गांधीजी की दृष्टि बहुत स्पष्ट थी। गांधीजी ने माना कि बालक-बालिकाएं जन्म से ही जिज्ञासु और सृजनशील होते हैं। यदि उन्हें अवसर दिया जाए तो वे खेल-खेल में बहुत कुछ सीख सकते हैं।
एक बालक जब मिट्टी से खिलौना बनाता है, तो उसमें उसकी कल्पनाशक्ति, धैर्य और श्रम का मूल्य छिपा होता है। जब तकली से सूत कातता है, तो वह धैर्य, अनुशासन और श्रम की महत्ता समझता है। जब अपने आसपास का परिसर साफ करता है, तो उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व और स्वच्छता का संस्कार आता है। इसीलिए गांधीजी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सोचने, खोजने और करने की प्रवृत्ति को पोषित करनाहै। दुर्भाग्यवश आज की शिक्षा प्रणाली गांधीजी की परिकल्पना से बहुत दूर निकल चुकी है। आज बच्चों पर सूचनाओं का बोझ लादा जा रहा है। पाठ्यक्रम खोज और जिज्ञासा की बजाय रट्टा लगाने पर आधारित हैं। प्राथमिक स्तर से ही प्रतियोगिता और अंक की दौड़ बच्चों का बचपन छीन रही है। आज शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व निर्माण न होकर मात्र नौकरी पाना रह गया है। यही कारण है कि लाखों युवक-युवतियां स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्रियां लेकर भी बेरोजगार हैं। उनके पास न तो व्यावहारिक कौशल है और न ही आत्मनिर्भर बनने की क्षमता। गांधीजी ने अपनी बुनियादी शिक्षा में श्रम और सृजन को केंद्र में रखा। उनका कहना था कि “हाथ का हुनर और दिमाग की समझ, दोनों शिक्षा का आधार हैं।” यदि बच्चा खेती करता है, तो उसे कृषि विज्ञान और प्रकृति से जुड़ाव दोनों की शिक्षा मिलती है। यदि वह बढ़ईगिरी, बुनाई, सिलाई, या लघु उद्योगों का अभ्यास करता है, तो उसमें आत्मनिर्भर बनने की शक्ति आती है। यदि वह चित्रकारी करता है, तो उसमें कला और सौंदर्यबोध का विकास होता है। गांधीजी की शिक्षा ‘पढ़ाई + काम’ का संतुलन थी। यह बच्चों को केवल कागजी डिग्री वाला नहीं, बल्कि जीवन जीने लायक कुशल और आत्मनिर्भर नागरिक बनाती थी।
आज हम बेरोजगारी, कौशल की कमी और शिक्षा के बाजारवाद की तीन बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। देखा जाए तो इन तीनों का समाधान गांधीजी की बुनियादी शिक्षा में छिपा है। यदि बचपन से ही बच्चों को स्वयं करके सीखने, हुनर अर्जित करने और सृजनशील बनने की शिक्षा मिले, तो वे स्नातक होते-होते नौकरी के मोहताज नहीं, बल्कि रोजगार सृजन करने वाले बन सकते हैं। वर्तमान शिक्षा नीति में “सामाजिक उपयोगी उत्पादक कार्य” को औपचारिक रूप से जोड़ा गया है। लेकिन यह विषय मात्र औपचारिकता रह गया है। बच्चे इसे गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि परीक्षा और अंकों से इसका सीधा संबंध नहीं होता। सच पूछा जाए तो गांधीजी के बुनियादी शिक्षा दर्शन को नीति-निर्माताओं ने केवल ‘पाठ्यपुस्तक की जानकारी’ बनाकर छोड़ दिया है। यदि इसे वास्तव में लागू किया जाए तो हर बच्चे को रोजाना व्यावहारिक कार्य का अवसर मिले,विद्यालयों में हस्तकला, कृषि, कला और विज्ञान आधारित परियोजनाएं अनिवार्य हों,
और शिक्षकों को इस दिशा में प्रशिक्षित किया जाए,तो भारत में बेरोजगारी और कौशल की कमी काफी हद तक दूर की जा सकती है। आज हमारी सरकारें आत्मनिर्भर भारत की बात करती है। आत्मनिर्भरता का यह विचार गांधीजी के बुनियादी शिक्षा दर्शन से ही निकला है। गांधीजी का कहना था- शिक्षा ऐसी हो जो बालक को अपने पैरों पर खड़ा कर सके। शिक्षा ऐसी हो जो बाजार पर निर्भरता कम कर सके। शिक्षा ऐसी हो जो समाजोपयोगी हो और ग्राम समाज को सशक्त करे। वास्तव में यदि हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो गांधीजी की इस शिक्षा को व्यवहार में लाना होगा। आज दुनिया “स्किल-बेस्ड एजुकेशन” पर जोर दे रही है। अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देश अपने बच्चों को बचपन से ही “करके सीखने” की शिक्षा दे रहे हैं। भारत में यह विचार गांधीजी ने 90 साल पहले रखा था। परंतु हमने इसे गंभीरता से लागू नहीं किया। यही कारण है कि भारत में आज भी कौशल की कमी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। आज जरूरत है कि शिक्षा नीति निर्माता गांधीजी की इस सोच को गंभीरता से अपनाएँ। विद्यालयों को केवल सूचना ठूंसने का अड्डा न बनाकर करके सीखने की प्रयोगशाला बनाना होगा। तभी भारत का युवा स्नातक होकर नौकरी की भीख मांगने वाला नहीं, बल्कि स्वयं रोजगार देने वाला बनेगा। वर्तमान समय और परिस्थितियों में गांधीजी का बुनियादी शिक्षा दर्शन केवल अतीत का स्मरण नहीं, बल्कि आज और आने वाले भविष्य की अनिवार्य आवश्यकता है।तभी हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करके सशक्त और समृद्धशाली भारत का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकेगें और यही गांधीजी को हमारी सबसे उपयुक्त श्रृद्धांजलि भी होगी।




